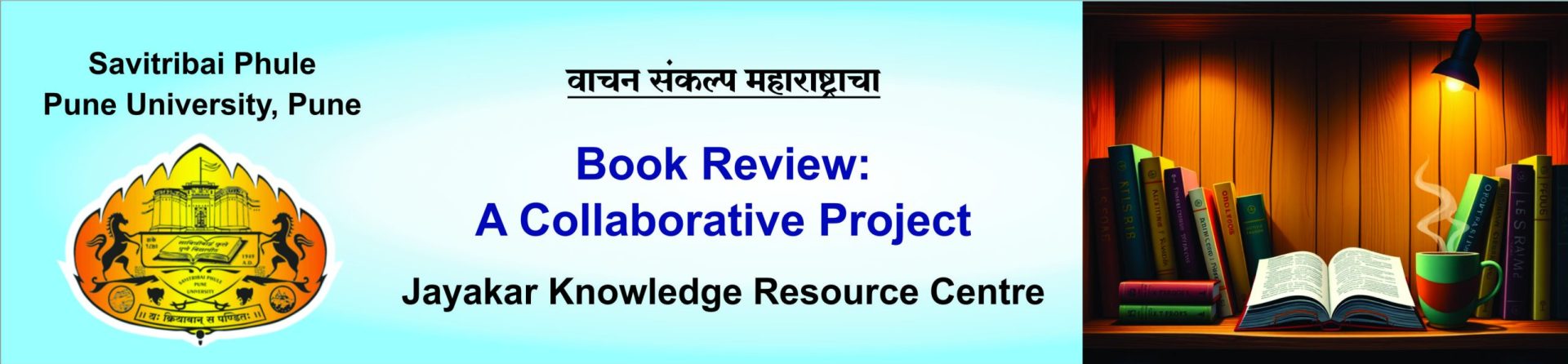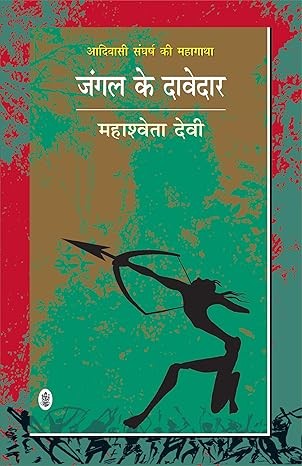
जंगल के दावेदार
Original Title
जंगल के दावेदार
Subject & College
Publish Date
2019-01-01
Published Year
2019
Publisher, Place
Total Pages
284
ISBN 13
978-8183611534
Language
हिंदी
Readers Feedback
जंगल के दावेदार
हँसते-नाचते-गाते, परम सहज आस्था और विश्वास से दी गई प्राणों की आहुतियों की महागाथा- जंगल के दावेदार ! आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा को इतिहासकारों ने...Read More
प्रा. कल्पना बागुल
जंगल के दावेदार
हँसते-नाचते-गाते, परम सहज आस्था और विश्वास से दी गई प्राणों की आहुतियों की महागाथा- जंगल के दावेदार !
आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा को इतिहासकारों ने अनदेखा किया होगा लेकीन महाश्वेता देवी ने उनके चरित्र पर उपन्यास लिखकर आदिवासी अस्मिता के प्रतिक को जिंदा रखा है. सुप्रसिद्ध बांग्ला कथाकार महाश्वेता देवी ने अपनी आत्मकथा तक में इसका जिक्र किया और लिखा कि सत्तर के दशक में साहित्यकारों एवं बंगाल के बुद्धिजीवियों के मानसिक नपुंसकता और अंधकार के क्षय का सबसे भयानक चेहरा हम देख सकते हैं. जहां देश और मनुष्य रक्ताक्त अभिज्ञता में जूझ रहे थे, वहीं बंगला साहित्य एक बड़े गंभीर दुख दर्द को छोड़कर परी देश के अलौकिक स्वप्न बाग में मिथ्या फूल खिलाने का ‘व्यर्थ’ आत्मघाती खेल में व्यस्त रहा गया था. बिरसा मुंडा का जन्म साल 1875 में रांची के लिहातु में हुआ था. यह कभी बिहार का हिस्सा था पर अब यह झारखंड में आ गया है. साल्गा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद बिरसा चाईबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ने आए. बिरसा मुंडा को अपनी भूमि, संस्कृति से गहरा लगाव था. कहते हैं जब वह अपने स्कूल में पढ़ रहे थे तभी मुण्डाओं, मुंडा सरदारों जमीन जबरिया छिनी जाने लगी. सुगना मुंडा और करमी हातू के पुत्र बिरसा मुंडा के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यहीं से विद्रोह पनपने लगा. यहीं से बिरसा मुण्डा आदिवासियों के भूमि आंदोलन के समर्थक बन गए. उनके भाषणों में, वाद-विवाद में आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर हक की वकालत बढ़ने लगी..और यहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का संघर्ष.
महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के इसी जीवन संघर्ष पर बंगला उपन्यास ‘अरण्यर अधिकार’ लिखा, जो हिंदी में ‘जंगल के दावेदार’ नाम से छपा. महाश्वेता देवी का यह उपन्यास केवल एक साहित्यिक, व्यक्तिपरक या ऐतिहासिक आख्यान भर नहीं है, इसका एक अलग महत्त्व है. उन्होंने बेबस आदिवासियों के बीच मिशनरी गतिविधियों के पाखंड को भी उजागर किया है कि कैसे एक पादरी डॉ नोट्रेट ने लोगों को लालच दिया कि अगर वह ईसाई बनें और उसके अनुदेशों का पालन करें तो वह मुंडा सरदारों की छीनी हुई जमीन वापस करा देगा. 1886 से 1890 तक बिरसा का चाईबासा मिशन के साथ रहना उनके व्यक्तित्व का निर्माण काल था. यही वह दौर था जिसने बिरसा मुंडा के अंदर बदले और स्वाभिमान की ज्वाला पैदा कर दी. मुंडा सरदारों ने जब 1886-87 में भूमि वापसी का आंदोलन किया, तो इस आंदोलन को न केवल दबा दिया गया बल्कि ईसाई मिशनरियों ने इसकी भी भर्त्सना की. बिरसा मुंडा की बगावत के पीछे की वजहों में एक वजह वादाखिलाफी व फरेब भी था. कहते हैं बिरसा के तेवरों को देखते हुए उन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया. 1890 में बिरसा तथा उसके पिता चाईबासा से वापस आ गए. बिरसा मुंडा पर संथाल विद्रोह, चुआर आंदोलन, कोल विद्रोह का भी व्यापक प्रभाव पड़ा. अपनी जाति की दुर्दशा, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अस्मिता को खतरे में देख उनके मन में क्रांति की भावना जाग उठी. उन्होंने मन ही मन यह संकल्प लिया कि मुंडाओं का शासन वापस लाएंगे तथा अपने लोगों में जागृति पैदा करेंगे. ‘जंगल के दावेदार’ बिरसा के इसी संघर्ष-यात्रा और अंग्रेजों के दमन की गाथा है. 25 वर्ष का अनपढ़, अनगढ़ बिरसा उन्नीसवीं शती के अन्त में हुए इस विद्रोह में संघर्षरत लोगों के लिए ‘भगवान’ बन गया था – लेकिन ‘भगवान’ का यह सम्बोधन उसने स्वीकार किया था उनके जीवन में, व्यवहार में, चिन्तन में और आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में आमूल क्रान्ति लाने के लिए. कोड़ों की मार से उधड़े काले जिस्म पर लाल लहू ज्यादा लाल, ज्यादा गाढ़ा दीखता है न! इस विद्रोह की रोमांचकारी, मार्मिक, प्रेरक सत्यकथा है- जंगल के दावेदार. हँसते-नाचते-गाते, परम सहज आस्था और विश्वास से दी गई प्राणों की आहुतियों की महागाथा- जंगल के दावेदार !